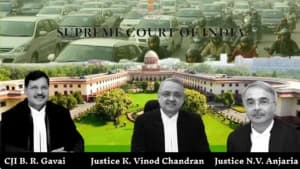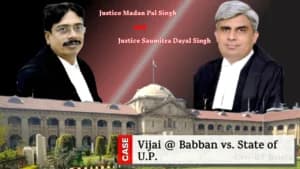उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर की गई आलोचना जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय की गई, ने तीखी प्रतिक्रियाएं जन्म दी हैं। उनकी टिप्पणी, जैसे "हाल ही के निर्णय में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं?" यह दर्शाता है कि मानो न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम रखा हो। लेकिन ऐसा कहना इस निर्णय की संवैधानिक व्याख्या को गलत तरीके से पेश करता है।
"अनुच्छेद 142 न्यायाधीशों के पास लोकतांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है।" – उपराष्ट्रपति धनखड़
इस प्रकार की भाषा आलोचना के बजाय दबाव की तरह लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया है कि राष्ट्रपति को उचित समयसीमा के भीतर निर्णय लेना चाहिए, जो कि लोकतांत्रिक जवाबदेही के अनुरूप है। यह सोचना कि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक समीक्षा से ऊपर हैं, पूरी तरह गलत है। पहले भी रमेश्वर प्रसाद (2006) और एस. आर. बोम्मई जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रपति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, भले ही उन्हें व्यक्तिगत मुकदमों से छूट हो।
Read Also:- कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की अनुच्छेद 142 पर टिप्पणी को बताया गंभीर, कहा - बेहद आपत्तिजनक
राष्ट्रपति कोई स्वतंत्र निर्णय लेने वाले संवैधानिक पदाधिकारी नहीं हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है। यह सलाह वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। वास्तव में, राष्ट्रपति की भूमिका राज्यपाल की तुलना में अधिक सीमित होती है। राज्यपाल के पास कुछ व्यक्तिगत विवेक के अधिकार होते हैं, जबकि राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की सलाह पर ही कार्य करना होता है।
“राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन माह के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है।” – सुप्रीम कोर्ट
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समयसीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं नहीं बनाई गई, बल्कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी 2016 को जारी मेमोरेंडम पर आधारित थी, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त विधेयकों को तीन महीने में निपटाने की सिफारिश की गई थी। सरकारिया और पुनचि आयोगों ने भी इस विषय में चिंता जताई थी।
यह कोई पहला अवसर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को निर्णय लेने की समयसीमा दी हो। शत्रुघ्न चौहान और बलवंत सिंह मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दया याचिकाओं पर उचित समय में निर्णय लिया जाना चाहिए, और विलंब के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया।
Read Also:- अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ 'परमाणु मिसाइल' बन गया है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाना चाहिए था। लेकिन जिन सिद्धांतों को लागू किया गया है, वे पहले से ही स्थापित हैं। शमशेर सिंह, एस.आर. बोम्मई, और हाल ही के पंजाब राज्यपाल मामलों में इन्हें पहले ही मान्यता दी गई है। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष ने यह अनुरोध नहीं किया कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए।
“सुनवाई के दौरान किसी ने भी इसे पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की मांग नहीं की।” – सुप्रीम कोर्ट
उपराष्ट्रपति की टिप्पणी यह सवाल भी उठाती है कि क्या विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखा जाना चाहिए? असल सवाल यही है। क्या बिना किसी कारण के विधायी प्रक्रिया को ठप किया जा सकता है? खुद केंद्र सरकार ने भी इस देरी पर चिंता जताई थी, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित है।
न्यायालय का निर्देश किसी भी तरह से लोकतंत्र पर हमला नहीं है, बल्कि यह संविधानिक प्रक्रिया को ठहराव से बचाने का उपाय है। यह निर्णय राष्ट्रपति के पद को कम करने के लिए नहीं बल्कि विधायी गतिरोध को रोकने के लिए है।
“यह निर्णय लोकतंत्र का अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक जड़ता का समाधान है।”