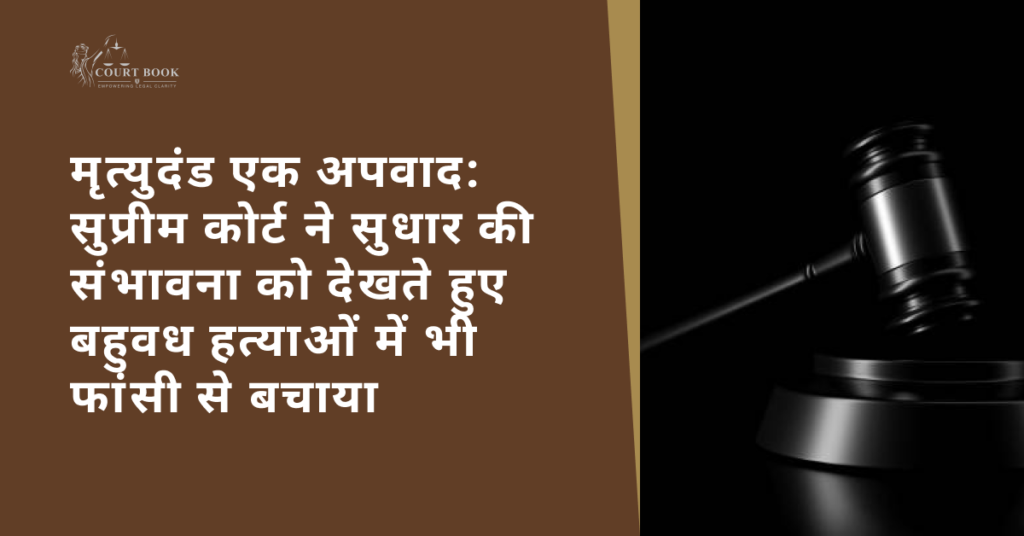सुप्रीम कोर्ट ने दीन दयाल तिवारी को उसकी पत्नी और चार नाबालिग बेटियों की क्रूर हत्या के दोषी ठहराए जाने को बरकरार रखा, लेकिन फांसी की सजा को बिना रिहाई के आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने बहुवध हत्याओं जैसे मामलों में भी सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना नवंबर 2011 में फैजाबाद (अब अयोध्या), उत्तर प्रदेश में घटी। तिवारी के भाई (पीडब्ल्यू-1) और भाभी (पीडब्ल्यू-2) ने रात के अंतिम पहर में उसके घर से चीखें सुनीं। वहां पहुंचने पर, उन्होंने दरवाजा बंद पाया और तिवारी को खून से सनी कुल्हाड़ी लिए बाहर आते देखा। पुलिस ने बाद में दरवाजा तोड़कर अंदर उसकी पत्नी और 3 से 10 साल की उम्र की चार बेटियों के शव पाए, जिन पर तेज धार वाले हथियारों के घातक चोटें थीं।
ट्रायल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत तिवारी को दोषी ठहराते हुए इस अपराध को "दुर्लभतम दुर्लभ" बताया और फांसी की सजा सुनाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हल्के करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए सजा पर पुनर्विचार किया।
कानूनी तर्क: फांसी की सजा क्यों बदली गई?
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिनमें तिवारी का खून से सनी कुल्हाड़ी लिए अपराध स्थल पर मौजूद होना, उसके बंद कमरे से हथियारों (कुल्हाड़ी और चाकू) का बरामद होना, और चिकित्सा रिपोर्ट्स द्वारा हथियारों से मेल खाती चोटों की पुष्टि शामिल थी। बचाव पक्ष ने फॉरेंसिक सबूतों में कमियां और एफआईआर में हेराफेरी का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मामूली विसंगतियां मुख्य सबूतों को कमजोर नहीं करतीं।
अपराध की भयावहता को स्वीकार करते हुए भी, कोर्ट ने हल्के करने वाले कारकों को रेखांकित किया, जैसे तिवारी का कोई पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना, उसका जेल में "संतोषजनक" व्यवहार, और पैरोल अधिकारियों द्वारा समाज में पुनर्वास की संभावना जताई जाना।
"यहां तक कि जहां बहुवध हत्याएं हुई हों, अगर सुधार का सबूत या संभावना हो, तो कम सख्त सजा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"
कोर्ट ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) का हवाला दिया, जो फांसी को उन्हीं मामलों तक सीमित रखता है जहां सुधार असंभव हो। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर (2010) और प्रकाश धवल खैरनार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) जैसे मामलों का उल्लेख किया, जहां पूरे परिवार की हत्या के बावजूद फांसी को आजीवन कारावास में बदला गया था।
Read Also - सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया
निर्णय से महत्वपूर्ण उद्धरण
सुधारात्मक न्याय पर कोर्ट ने कहा,
"संविधान अपराध और अपराधी दोनों की जांच मांगता है। गंभीर मामलों में भी दोषी के सुधार की क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।"
सामाजिक प्रभाव पर कोर्ट ने टिप्पणी की,
"हालांकि अपराध समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देता है, सजा को समाज के हित और दोषी की मानवता के बीच संतुलन बनाना चाहिए।"
Read Also - राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय: योग खेल नहीं, पीटी प्रशिक्षक चयन में बोनस अंक नहीं
यह फैसला स्थापित करता है कि भविष्य के मामलों में क्रूरता और पीड़ितों की संवेदनशीलता जैसे गंभीर कारकों के साथ-साथ आयु और सुधार की संभावना जैसे हल्के करने वाले कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अदालतों को फांसी से तब तक बचना चाहिए जब तक कि पुनर्वास पूरी तरह असंभव न हो, और स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2008) जैसे पूर्व निर्णयों के अनुसार घोर अपराधों के लिए बिना रिहाई के आजीवन कारावास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
तिवारी का दोष सिद्ध होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसमें रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह फैसला मृत्युदंड को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के साथ मेल खाता है और भारत के मानवीय न्याय के प्रति समर्पण को पुष्ट करता है।
मामले का नाम: दीन दयाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 2220-2221/2022